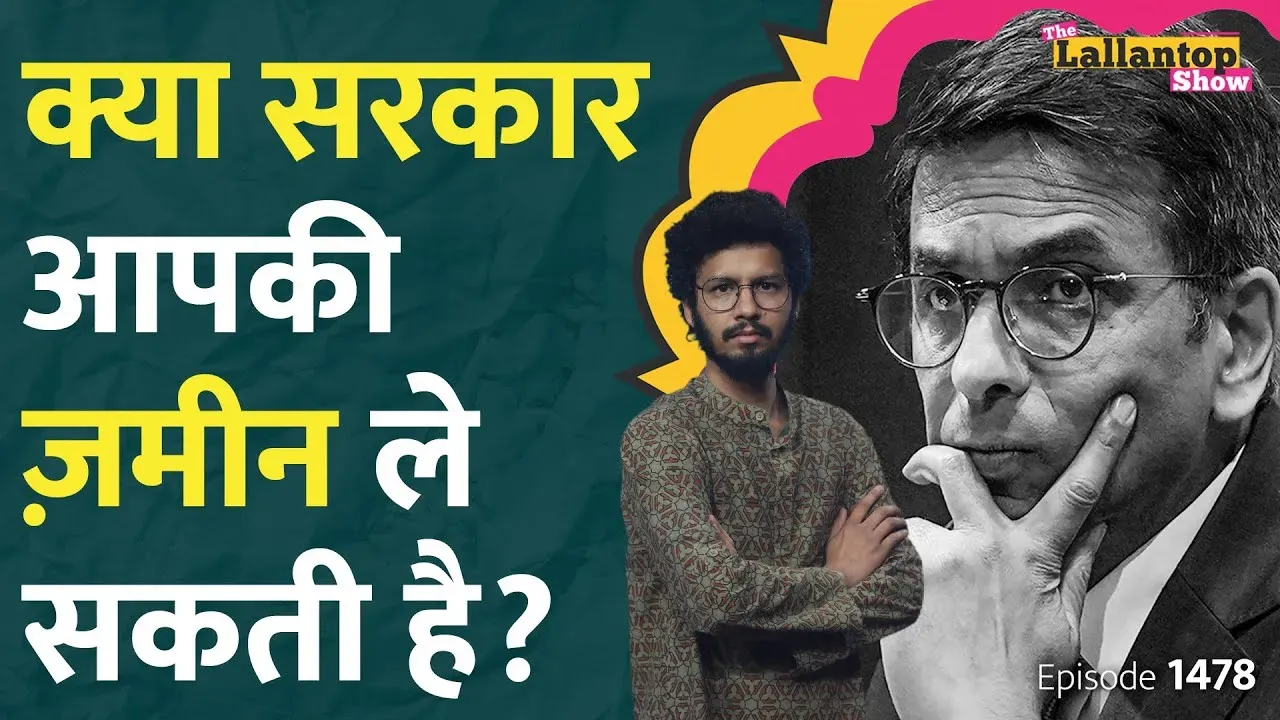सबसे पहले एक तस्वीर देखिए.
रिव्यू - 'गांधी-गोडसे: एक युद्ध'
फ़िल्म के आख़िरी सीन को छोड़ दें, तो गांधी पूरी फ़िल्म में एक 'बिगर पर्सन' ही दिखते हैं.


ये तस्वीर हमारे साथी अनुभव ने खींची है. जगह: इंडियन कॉफ़ी हाउस, इलाहाबाद. जब से ये इमारत है, तब इलाहाबाद ही था. एक पुरानी दरकती इमारत, जो कभी उत्तर भारत में राजनीति और साहित्य का केंद्र हुआ करती थी. नेहरू के ज़माने में, फ़िराक़ के ज़माने में, हरिवंश राय बच्चन के ज़माने में. तीनों ही गांधीवादी थे. इस देश में सबके अपने गांधी हैं. किसी के लिए 'राष्ट्रपिता', किसी के लिए 'बंटवारे का ज़िम्मेदार'. अनुभव के भी अपने गांधी हैं. और, राजकुमार संतोषी के भी. 'गांधी-गोडसे: एक युद्ध' वाले गांधी. राजकुमार संतोषी ने इस फ़िल्म के ट्रेलर लॉन्च में कहा था कि वो 9 साल बाद आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है. क्या लेकर आ रहे हैं, ये ज़रूरी है. हमने उनकी पिक्चर देख ली. क्या लाए हैं, ये बताते हैं.
फ़िल्म में उतरने से पहले: वक़्त के हिसाब से, फ़िल्म कुछ-एक से ज़्यादा लोगों को आहत कर सकती है. लेकिन ये एक ज़रूरी फ़िल्म है, जो संवाद में सिंसयर भरोसा रखती है.
मेरे जीवन में गांधी कैसे आए? 2 अक्टूबर की छुट्टी से. स्कूल की किताबों से. दफ़्तरों की दीवार पर टंकी तस्वीरों से. चौराहों पर लगी मूर्तियों से. रुपए के नोट से. निबंध और भाषण के विषयों से. 'लगे रहो मुन्ना भाई' से. वॉट्सऐप और यूट्यूब से. सत्य के साथ उनके प्रयोग से. इधर-उधर के लेखों से. और, ट्विटर से. ठीक इसी क्रम में. जितने आए, वो ये कि एक दमदार बूढ़ा आदमी है. जिसे लोग 'महात्मा' कहते हैं, क्योंकि उसे मनुष्य कहने से झेंपते हैं. वो हठी है; ग़लती करता है. ग़लतियां स्वीकारता है. अपने विचारों पर दृढ़ है, लेकिन खुलता रहता है. पक्का वैष्णव है. पढ़ा-लिखा व्यक्ति है. कभी वकील रहा. उतना 'भोला' है नहीं, जितना समझा जाता है.
राजकुमार संतोषी को भी कुछ-कुछ ऐसा ही लगा. उन्होंने गांधी को बख़्शा नहीं है. उन्हें 'राष्ट्रपिता' होने का प्रिवलेज नहीं दिया. न गोडसे के पक्ष में रहने का प्रयास किया, न गांधी के. मुद्दे को डॉयकॉटमी या द्विधाकरण में नहीं ले गए. दो विचारों का आमना-सामना करवाया है.

30 जनवरी 1948. नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी. 75 साल बाद इसी दिन के चार दिन पहले ये फ़िल्म आई है.
फ़िल्म का कॉन्सेप्ट बेजोड़ लगा. मैंने ट्रेलर नहीं देखा था, तो प्रयोग के लिहाज से मेकर्स का काल्पनिक विस्तार ग़ज़ब लगा. अगर गांधी गोडसे की गोलियों से ज़िंदा बच जाते, तो क्या होता? क्या करते? कांग्रेस के साथ क्या करते? सरकार के प्रति उनका क्या रुख रहता? अपने हत्यारे नाथुराम गोडसे से बात की होती, तो क्या बात होती? फ़िल्म ने इन सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है. हो सकता है कुछ जगहों पर आप उनकी कल्पना से इत्तेफ़ाक़ न रखें, मगर कल्पना की ख़ूबसूरती यही है. कुछ भी सोच सकते हैं.
जब उस सोच पर फ़िल्म बनानी हो, तो मेकर्स उस सोच को पॉलिश करते हैं. एक नैरेटिव देते हैं. 'यूं होता तो क्या होता' पुराना शगल है. लेकिन इसमें हमेशा ही रिस्क रहता है, कि आप किसी की तरफ़ दिखने लगते हैं. मेकर्स ने प्रयास किया है कि इससे बचें. फ़िल्म के आख़िरी सीन को छोड़ दें, तो गांधी पूरी फ़िल्म में एक 'बिगर पर्सन' ही दिखते हैं.
वैसे इस सोच का पूरा क्रेडिट जाता है प्ले-राइट और स्क्रीन-राइटर असग़र वजाहत को, जिनके नाटक पर ये फ़िल्म बनी है. असग़र वजाहत ने ख़ुद इस फ़िल्म में डॉयलॉग्स लिखे हैं. राजकुमार संतोषी के साथ.

फ़िल्म की बेस-लाइन ये है कि गांधी से जुड़े सारे कंटेंपरेरी आरोपों और बहसों को अड्रेस किया जाए. मसलन, गांधी का बोस के लिए क्या रवैया था? नेहरू और पटेल के बारे में क्या सोचते थे? बंटवारा किसने करवाया? अखंड भारत पर क्या सोचते थे? कुल मिलाकर बात ये कि पिछले कुछ सालों में वॉट्सऐप पर जो भी आरोप लगे, गांधी उससे कैसे डील करते?
गोडसे को एक अडिग हिंदू का ही रोल दिया गया है. उसके अपने विचार थे. उसने इंपल्स में गोली नहीं चलाई थी. वो समझता था कि उसका क़दम देशहित में है. उसे लगता था कि गांधी ओवर-रेटेड हैं. देश को अपनी सोच पर चला रहे हैं, किसी की नहीं सुनते, सबसे ऊपर हैं. ये भी सोचता था कि केवल कॉन्ग्रेस और गांधी ने देश को आज़ादी नहीं दिलाई. भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई लोगों ने क़ुरबानी दी; गोली खाई.
तब भी गांधी को हिंदू विरोधी, अंग्रेज़ों का एजेंट, मुसलमान प्रेमी और बंटवारे का ज़िम्मेदार कहा जाता था. तब भी ऐसी बातें होती थीं की गांधी ने अहिंसा और चरखे में उलझा दिया है. गर्म दल को समर्थन मिलता, तो 20 साल पहले ही आज़ादी मिल जाती. और, गांधी को इन सवालों के साथ कनफ़्रंट किया गया है.

फ़िल्म के संवाद अनुपम हैं. लिखाई की नज़र से नहीं, मुद्दे की नज़र से. गांधी और गोडसे का एक संवाद है, जिसमें गोडसे उन्हें अखंड भारत का नक्शा दिखाता है और कहता है कि उसका सपना है अखंड भारत. गांधी मुस्कुरा के पूछते हैं, "तुमने इस नक्शे में तिब्बत, बर्मा और अफ़ग़ानिस्तान को भी शामिल कर लिया है. तुम कभी वहां गए हो? क्या उनकी संस्कृति के बारे में जानते हो?" गोडसे चुप हो जाता है. क्यों भाई, जानते हो?
ख़ैर. फ़िल्म में गांधी और उनके कांग्रेस से मोहभंग की बात भी बताई गई है. गांधी ने अपने जीते जी कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी. उनका मत था कि कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए एक खुला मंच था, अब इसके नाम पर लोगों से वोट मांगना ठीक नहीं है. एक संवाद में गांधी कहते हैं:
"सरकारें सेवा नहीं करतीं. केवल हुक़ूमत करती हैं."
साइकोलॉजी में एक पुरानी पंक्ति चलती है - 'पावर करप्ट्स'. यानी ताक़त का बेसिक नेचर है कि वो आपको भ्रष्ट कर देती है. गांधी प्रतीक हैं कि असीम ताक़त होने के बावजूद उसे एक्सप्लॉइट करने की कोई वजह नहीं हो सकती. उस व्यक्ति के एक इशारे पर सरकार बन सकती थी, गिर सकती थी. अगर वो अपनी सरकार से ही तन जाते, तो एक और जनांदोलन हो जाता. लेकिन उन्होंने किसी पर एक पत्थर नहीं चलाया. किसी पर हाथ नहीं उठाया.

फ़िल्म में गांधी और गोडसे, दोनों को खुलते हुए दिखाया गया है. कैसे वो दोनों एक-दूसरे की सोहबत में रहकर कुछ-कुछ बदले. केवल गोडसे नहीं, गांधी भी.
दो-एक और प्रयोगसिनमैट का काम अव्वल है. कैमरे का काम फ़िल्म के नैरेटिव के साथ घुला हुआ लगता है. एकाध शॉट्स बहुत ही बारीक़ी से बनाए गए हैं.
ऐक्टर्स की बात देर से हो रही है, इसके लिए माफ़ी. मगर विषय को तवज्जो देना ज़रूरी थी. गांधी के रोल में दीपक आंतनी का काम जानदार है. ख़ैर, गांधी का रोल प्ले करने में वो पारंगत हैं. पहले भी कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने गांधी का रोल किया है. वो मोहनदास करमचंद गांधी के नुआंसेज़ पकड़ते हैं. गोडसे का किरदार किया है चिन्मय मांडेलकर ने. माने हुए ऐक्टर हैं. पहले भी अच्छा काम किया है, और इस रोल के साथ भी जस्टिस करते हैं. बाक़ी कैबिनेट ने भी अपना योगदान कैबिनेट-नुमा ही दिया है.
दो-एक सीन बहुत ही ज़रूरी हैं. जैसे कैबिनेट सहित गांधी कुछ रजवाड़ों से मिलने आते हैं. स्वाभाविक है कि क़ानून मंत्री बाबा साहेब भी आए थे. उनका संवाद तो दमदार है ही, जाने के बाद वो रजवाड़े अपने घर में हवन करवाते हैं. जातिवाद की तब की स्थिति को दिखाने का बहुत सटल प्रयास है. और, आपको स्पून-फ़ीड नहीं किया जाता कि देखो, आम्बेडकर आए थे, इसलिए शुद्धी हवन हो रहा है. वो नेपथ्य में है, लेकिन साफ़-साफ़ दिख रहा है.

फ़िल्म का आख़िरी सीन सांकेतिक तौर पर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं उससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखता. चाहते-न चाहते उसमें गांधी और गोडसे को सम पर ला दिया गया है. जिससे मेरी असहमति है. आपकी नहीं भी हो सकती है.
बाक़ी, पिक्चर बढ़िया है. देख डालिए.
वीडियो: क्या महात्मा गांधी ने भगत सिंह को 'जानबूझकर' नहीं बचाया?


















.webp)

.webp)